'लगान' में मुखिया , 'पान सिंह तोमर' में मेजर रंधावा, 'बालिका वधू' में महावीर सिंह, 'चिड़ियाघर' में केसरी नारायण , 'कहानी चंद्रकांता की' में पंडित जगन्नाथ... नाम अलग-अलग हैं लेकिन कलाकार एक ही है ।
राजेन्द्र गुप्ता ने पानीपत से दिल्ली, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और फ़िर बालीवुड तक के सफर पर मधु अरोड़ा से जो गुफ्तगू की, उसे आप तक ला कर, शब्दांकन अपना योगदान दे रहा है ...
आपके लिये नाटक क्या है?
आज मैं जो कुछ भी हूं, नाटक की वज़ह से ही हूं। मैं जब नाटक सीखने
एन एस डी गया तो वहां नाटक को सीखा, उसे समझा और जब मंच पर नाटक किये तो मुझे लगा कि मैं नाटक के लिये ही बना हूं और सच कहूं तो वहां एक तरह से ख़ुद को पाया था। एन एस डी में नाटक सीखने के दौरान ही कहानी और निर्देशन की समझ आयी। अपनी शिक्षा के दौरान मैं विज्ञान का छात्र रहा, साहित्य का छात्र तो कभी रहा नहीं। सो नाटक-कला को सीखते समय ही साहित्य को समझने की समझ आयी। धीरे-धीरे नाटक करने में मज़ा आने लगा और फिर तो नाटक में इस तरह डूबता चला गया कि उससे बाहर आना संभव ही नहीं था। अब जब से मैं सीरियल और फिल्में करने लगा हूं तो नाटक और भी ज़रूरी लगने लगा है। नाटक आपको साहित्य से जोड़ता है। जब तक कला साहित्य से नहीं जुड़ेगी, वह आपको इन्वाल्व नहीं कर सकती। नाटक का महत्वपूर्ण तत्व लेखन है लेकिन आज के आपाधापी के दौर में वह ग़ैर ज़रूरी हो गया है। हां, तो मैं कह रहा था कि आज मेरा जो व्यक्तित्व है, वह नाटक के कारण है। मेरे व्यक्तित्व को बनाने, संवारने का श्रेय नाटक को जाता है।
आप तो संपन्न परिवार से हैं फिर आपने संघर्ष का रास्ता क्यों चुना?
कोई भी जानबूझकर संघर्ष का रास्ता नहीं चुनता। आप करते बहुत सारे काम हैं, पर अपनाते वही हैं जिसमें आपको मज़ा आता है। मैंने भी बहुत ग़लतियां कीं, बहुत भटका, बहुत तथाकथित संघर्ष किया, पर घूम-फिरकर जब नाटक में आया तो मुझे असली मज़ा आया इसमें। दूर से कई चीजें आसान लगती हैं, वह तो उस क्षेत्र में आने पर पता चलता है कि कितने मुश्किलात हैं इधर। आपको तो पता है कि इन्सानी नेचर ऐसा नहीं होता कि वह सुविधाओं को छोड़ दे। मैं मानता हूं कि संघर्ष जैसा कोई शब्द है ही नहीं। जब हम किसी काम को अपनी मर्जी़ से चुनते हैं तो संघर्ष किस बात का? लेकिन इन्सान ज़बर्दस्ती ग्लोरिफाई करता है अपने संघर्ष को। अन्तत: तो यह आपका अपना मज़ा ही है। माना, फिल्मों में पैसा है, शोहरत है लेकिन आपका ताल्लुक़ आन्तरिक सुख से है। आन्तरिक सुख तो एक मृगतृष्णा है, उसकी तलाश में हम नये-नये काम करते हैं और अपनी प्रतिभा को तराशते हैं। बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। हरेक का अपना तरीका है ख़ुद को अभिव्यक्त करने का। अपने सुख के लिये काम की तलाश को आप संघर्ष कह लीजिये या कुछ और। अंतत: तो यह आपका और सिर्फ़ आपका अपना मज़ा है।
आप मुंबई किस प्रयोजन से आये?
मैं भी उन हज़ारों लोगों में से हूं जो काम की तलाश में मुंबई आते हैं। नाटक तो मैं दिल्ली में भी करता था लेकिन मुंबई में सिनेमा भी था और नाटक भी था। एक बात यह भी थी कि जब हम नाटक करते थे, तो नाटक के लिये ही नाटक करते थे। परन्तु इन्सान आन्तरिक उन्नति के साथ-साथ बाहरी उन्नति भी तो चाहता है न! दिल्ली में इस तरह की संभावना दिखती नहीं थी। दिल्ली में नाटक करना मेरी तात्कालिक स्थितियां थीं। मैं उन दिनों
पानीपत में रहता था तो 200 किलोमीटर की दूरी थका देती थी। ऐसे में लगता था कि यह प्रोडक्टिव नहीं है। मुझे लगता था कि मैं किसी लायक नहीं हूं। मेरे साथ एक दिक्कत थी और अभी भी है कि कोई मुझे लंबे समय तक पकड़कर नहीं रख सकता था। मुझे महसूस हुआ कि मैं नाटक के लिये ही बना हूं और बेहतरी के लिये मुंबई शिफ्ट कर लिया। सोचा कि जब यही करना है तो जो भी होगा, देखा जायेगा। जब शिफ्ट करना ही है तो क्यों न मुंबई जाया जाये। मेरे लिये दिल्ली/मुंबई बसना एक ही बात थी। सो इस तरह पत्नी
वीना और छोटे-छोटे दो बच्चों के साथ मुंबई चला आया। अकेला कभी नहीं गया। अपने परिवार को हमेशा अपने साथ रखा।
संघर्ष आपकी पीढ़ी को भी करना पड़ा था और संघर्ष आज की पीढ़ी को भी करना पड़ रहा है। इन दोनों संघर्षों में आप क्या फर्क़ पाते हैं?
मैंने इस पर ग़ौर से स्टडी नहीं की है।
संघर्ष बड़ा व्यक्तिगत सा होता है। संघर्ष करना इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का नेचर, ज़रूरतें और व्ख़ाब क्या हैं?
संघर्ष यह भी है कि एक नौकरी मिल जाये और रोज़ी-रोटी का जुगाड़ हो जाये। संघर्ष यह भी है कि फिल्मों में, सीरियलों में रोल चाहिये। इसके लिये आप फोटो खिंचायेंगे, फोटो सेशन करायेंगे। दरअसल किसी भी कार्य में हमारा पारिवारिक माहौल बहुत काम करता है। हमारे रहन-सहन, बोल-चाल, खान-पान के ढंग से पारिवारिक पृष्ठभूमि सामने आती है।
इंसान की हर चीज़ बहुत व्यक्तिगत होती है। यह अलग बात है कि हर चीज़ को जनरलाइज करने के लिये हम कुछ भी बोल जाते हैं।
अब रही बात पहले की पीढ़ी और और आज की पीढ़ी के संघर्षों में फर्क़। तो मधुजी, मेरी पीढ़ी के लोग काफी साल पहले ही मुंबई आ गये थे और मैं एनएसडी से उत्तीर्ण होकर काफी साल बाद मुंबई आया था। मुझे सोचना पड़ता था कि मुझे मुंबई जाना है। एक तरफ मुंबई जैसा शहर आपको जितना आकर्षित करता है, उतना ही डराता भी है। सो पत्नी से विचार-विमर्श करके ही मुंबई आया। पत्नी के समर्थन के बिना तो बिल्कुल भी नहीं आता। हां, यह बात ज़रूर थी कि मुझे खाने-पीने के इंतजाम की चिन्ता नहीं थी। उस सबकी व्यवस्था आराम से हो जाती थी। मग़र, आज एन एस डी का बच्चा बहुत जल्दी मुंबई आ जाता है। इसका मतलब है कि टी वी के कारण इतनी ओपनिंग हो गई है कि संघर्ष कम हो गया है। आपके सीनियर साथी आपके संघर्ष को कम करते हैं। वे आपके लिये सीनियर एंकर होते हैं। वे आपका मार्गदर्शन करते हैं। हमारे समय में ऐसा नहीं था। एन एस डी से पास करके छात्रों को अकेले आना होता था और अकेले संघर्ष करना होता था। कोई मार्गदर्शन करनेवाला नहीं होता था। उस समय संघर्ष तो थे पर रास्तों का पता नहीं होता था कि किस राह पर चलकर मंजि़ल पाना है।
आप अपने संघर्ष को किस तरह तरह देखते हैं?
आप तो जानती हैं कि हर व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाश है।
कला में रोज़ी-रोटी पाना मुश्किल होता है और यह मुश्किल बनी रहती है।
यह व्यक्ति पर निर्भर होता है कि वह किस बेहतर की तलाश में है। फिल्मों, सीरियलों में जितने अवसर बढ़ रहे हैं, डिमांड भी बढ़ रही है तो आपसी प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है। सबको अपने क्षेत्र में काम करना आता है लेकिन इस चक्रव्यूह को कौन तोड़े? जो इस चक्रव्यूह को तोड़ने में माहिर है, वह आगे बढ़ जाता है। तो यह सब संघर्ष ही है और चलता रहेगा। यह बात अलग है कि कोई संतुष्ट हो जाता है और कोई इस संतुष्टि को लगातार तलाशता है। मैं अपने काम से कभी संतुष्ट नहीं होता बल्कि लगता रहता है कि कुछ कमी है। जब मैं मुंबई आया था तो मारूति कार लेकर आया था। तो इस बात पर लोग हंसते भी थे और जलते भी थे। लेकिन मेरा जो संघर्ष तब था, वही आज भी है। हां, वे लोग बहुत आगे बढ़ गये, पर मैं वहीं हूं। जिन्होंने मुझे शुरू से देखा है, वे जानते हैं कि मैं वही हूं, वहीं हूं।
आप नाटकों, फिल्मों और सीरियलों से ग़हराई से जुड़े हैं, किस विधा में आप ख़ुद को सहज पाते हैं?
दरअसल, सहज महसूस करना कोई मायने नहीं रखता। आपको पता है कि नाटकों, फिल्मों और सीरियलों के अलग- अलग अनुभव, अलग-अलग कारण और अलग- अलग सुख हैं।
हम सिनेमा इसलिये करते हैं ताकि हमारा काम ज्य़ादा लोगों तक पहुंचे और नाम भी पहुंचे और उसीके जरिये फाइनेंशियल इमेज पहुंचती है। हमारी व्यावसायिक इमेज बन जाती है। यह इसका एक पहलू है। हम सीरियल तब करते हैं जब सिनेमा में उस शीर्ष तक नहीं पहुंच पाते।
अभिनय हम सीरियल में भी करते हैं। इससे अभिनय भी हो जाता है और एक तयशुदा रक़म भी मिल जाती है और सबसे बड़ी बात कि हम ख़ुद को बेकार महसूस न करें, विशेष रूप से सामाजिक रूप से। हां, सीरियलों के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं।
मैं मानता हूं कि मुझे सीरियलों अच्छे रोल मिले हैं, सिनेमा में नहीं।
एक बात यह भी है कि सिनेमा व सीरियलों में वहां की कंडीशन, कंपल्शन्स में काम करना होता है। जबकि थियेटर में हमें स्वयं को मांजने का, रियाज़ करने का मौका मिलता है। अपने काम के नये रूप ढूंढ़ने का, आत्म संतुष्टि का, चुनौतियों का सामना करने का मौका नाटक में मिलता है। हम तीस से साठ दिन लगातार अपने को-स्टार्स के साथ काम करते हैं, उस चरित्र को जीने की अभिव्यक्ति में उतारने का अंदाज़ थियेटर देता है। हम नाटक को मिल-जुलकर करते हैं और कार्य को जीवन में उतारने के लिये मेहनत करते हैं। Constant प्यास के तौर पर फिल्म करते हैं। मेरा मुंबई आने का अभिप्राय फिल्में भी था। नाटक तो दिल्ली में भी कर रहे थे। एक अच्छे नाटक की की संतुष्टि आंतरिक है जो सिनेमा, सीरियल में कभी ही मिलती है। इच्छा है उन क्षणों को जीने की जो मुझे, आपको और लोगों को मज़ा दे।
फिल्मो में भाषा की गिरावट के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्मों में वह भाषा है जो लेखक, डाइरेक्टर ने दी है। एक्टर उनकी संतुष्टि के लिये कार्य करता है और उसे करना पड़ेगा, चाहे वह ग़लत ही क्यों न हो। आपके और मेरे लिये जो कुभाषा है, वही उनके लिये भाषा है। आप ही बताईये, हमारे पास अपने जो संस्कार हैं, नाटक के जो अनुभव हैं, जो भाषा है ये सब कहां जायेंगे? उसे हम कैसे भुला पायेंगे? ऐसा तो मुझे कभी कोई कारण नहीं मिला कि इस भाषा को छोड़कर उस भाषा को पकड़ूं।
कुछ वर्षों से आपके आंगन में चौपाल का आयोजन हो रहा है, तो चौपाल का ख़याल आपके मन में कैसे आया?
कहीं न कहीं अवचेतन मन में मिल-बैठकर बतियाने की तमन्ना थी। हम जिस तरह की जि़न्दगी जीते हैं उसमें थियेटर में भी उतने मौके नहीं मिल पाते। नाटक का सूत्रधार, निर्देशक, लेखक एक ही व्यक्ति होता है। वह आल इन वन काम करता है। वह अकेला पूरी संस्था चलाता है। हिंदी नाटक के कुल जमा चार- पांच ही ग्रुप हैं। हमेशा यह ज़रूरी नहीं होता कि हम उसी ग्रुप के साथ काम करें। मेरे पास संस्था चलाने की कूवत नहीं है। प्रमुख रूप से मेरे अन्दर एक्टर है। चौपाल शुरू होने से पहले की बात है, हम लोग इकठ्ठे बैठकर कभी-कभी नाटक पढ़ते थे। ख़ुद से जुड़े रहने के लिये, अपनी आत्मा की ख़ुराक के लिये यह ज़रूरी लगा। चौपाल शुरू करने का श्रेय शेखरसेन को जाता है1 उन्होने चौपाल के आयोजन का सपना दिखाया, विचार दिया और उनके इस विचार और सपने को 1998 में चौपाल को शुरू करके कार्यरूप दे दिया गया और इस प्रकार चौपाल का जन्म हो गया। मुझे याद आता है कि 27 जून, 1998 को कालिदास जयन्ती थी। उस दिन आषाढ़ का एक दिन नाटक और मेघदूत आदि पढ़े गये। हमने ही अपने- अपने पांच-पांच लोगों को आमंत्रित कर लिया और आगे चलकर इसे अच्छा सहयोग और ज़बर्दस्त समर्थन मिला। फिर धीरे-धीरे काम बांटते चले गये और अब महीने में एक बार चौपाल जमती है। मेरा इसमें सहयोग कम है। इसकी जि़म्मेदारी संभालनेवाली त्रिमूर्ति है- शेखरसेन, अतुल तिवारी और अशोक बिन्दल। ये लोग आउट आफ वे जाकर काम करते हैं। ये लोग चौपाल के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और उन्होने इसे महत्वपूर्ण माना है। जो इस चौपाल में आते हैं, उनका जिस तरह से साथ मिलता है, वह अभूतपूर्व है। हम एक-दूसरे को चौपाली कहते हैं। चौपाल को शुरू हुए चौदह वर्ष हो गये।
आप अभी हाल में एक ग्रुप के साथ फैज़ पर आयोजित कार्यक्रम हेतु पाकिस्तान गये थे, वहां का अनुभव कैसा रहा?
यह अनुभव अपने आप में अद्भुत था। हम लोग वहां पांच दिन थे। बहुत ही मज़ा आया। हमारे दिलों में सामाजिक, राजनैतिक ख़बरों की वजह से जो टोटल पर्सपैक्शन बस गया है, जिसमें दुश्मनी दिखती है, उससे एकदम सौ प्रतिशत उलट अनुभव मिलते हैं, वहां जाकर व्यक्तिगत तौर पर।
मेरे जैसा व्यक्ति सोचता है कि दोनों देशों के द्वारा फैलाया गया यह षणयंत्र का जाल है ताकि उनकी गद्दियां बची रहें।
उन्होने हमें जो सम्मान दिया, उससे भ्रान्तियां टूटती हैं। उनकी भी हमारी जैसी संस्कृति, सरोकार और भावुकता है। हमारे यहां किसी कवि को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं होता जबकि हमारे यहां उनके बनिस्बत ज्य़ादा खुलापन है। वहां फैज़ का म्यूजियम है, लायब्रेरी है जो जनता के लिये खुली है। अपने यहां ऐसे बहुत से घराने, परिवार हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर किसी ने हमारे लेखकों के लिये कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। हमें साहित्य के जरिये उन लोगों में घुसपैठ करनी चाहिये और अपने यहां भी ऐसे काम होने चाहिये। हम बारह लोग वहां गये तो यदि हम उनका सद्व्यवहार बारह सौ लोगों तक भी पहुंचा सकें तो हमारे बीच के पूर्वाग्रह कम हो सकेंगे और एक दूसरे को स्वीकार करने की क्षमता विकसित कर सकेंगे1 यदि हम यह आना- जाना शुरू कर दें तो इसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन…
थियेटर ने आपको नाम, ख्याति, स्थायित्व और पहचान दी है। सुना है, आपको जीवनसाथी भी थियेटर ने दिया है?
जी, नाटक की दुनिया ने पत्नी दी है, नाटक ने नहीं। मैं नाटक-यात्रा के दौरान उज्जैन में 'अंधा युग' नाटक कर रहा था, जिसमें वीना के रिश्तेदार काम कर रहे थे। उनके जरिये वीना से मुलाक़ात हुई, वह नाटक की देन हैं।
आपकी पत्नी आपकी सहयोगी ही बनीं या कभी रूकावट भी बनीं?
वीना ने हमेशा मेरा साथ दिया है1 उन्होने दिल से, पूरी तरह से साथ दिया है। सचमुच Big support. उन्होने बख़ूबी घर की जि़म्मेदारी, बच्चों की जि़म्मेदारी संभाली। मुझे लगता है कि यह प्लस पांइट हो जाता है आपके काम में। हम तो एक दूसरी दुनिया से आये लोग हैं जिन्हें 'परिवार' पता नहीं होता। धीरे-धीरे स्वीकारोक्ति होती है और इसमें वीना काफी पाजिटिव रही।
संबंधों को बनाने, सहेजने में आप ख़ुद को कितना सहज महसूस करते हैं?
मैं बहुत सहज और असहज दोनों हूं। मुझसे संबंधों में पहल नहीं हो पाती है। सहज संबंध अपने आप बन जायें तो बन जाते हैं और फिर बहुत लंबे तक चलते हैं। मेरे सोशल संबंध नहीं होते। मुझसे परिचय बढ़ानेवाले संबंध नहीं बन पाते। आप ग़ौर करती होंगी कि मैं चौपाल में भी ज्य़ादा ग़ुफ्तगू नहीं कर पाता। जब तक परिचय औपचारिक रहता है, निजी नहीं होता तो बहुत समय लगता है सहज संबंध बनाने में। गोष्ठियों, पार्टियों में मिले परिचय संबंध का रूप ले ही नहीं पाते। मेरे लिये पर्सनल बात बहुत ज़रूरी है याने वन-टू-वन बातचीत। मेरा मेमोरी सिस्टम बहुत ख़राब है जिसके कारण मुझे जल्दी कुछ याद नहीं आता। दूसरे, हर आदमी की सोच अलग होती है। यदि इसे स्वीकार कर लें तो दुनिया आसान हो जायेगी। जैसे चेहरे अलग-अलग हैं, वैसे ही सोच, इच्छाएं, प्रमुखताएं अलग-अलग हैं। मज़े, शौक, सरोकार सब कुछ अलग हैं। इसलिये जनरल न कुछ कह सकते हैं और न कर सकते हैं। कामन फैक्टर्स को निकालकर एक रूप दे दिया जाये, यह जुदा बात है। गणित, फिजिक्स के नियम जनरल हैं, ये पढ़ाये जा सकते हैं, लेकिन मानव स्वभाव! ये सबसे परे है।
शब्दांकन के लिये मुंबई से मधु अरोड़ा
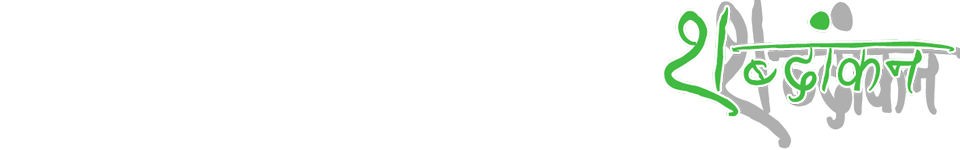


















0 comments:
Post a Comment