"मेरे नारी चरित्र सुन्दर होते नहीं, सुन्दर प्रतीत होते हैं" - मनीषा कुलश्रेष्ठ

आज के सफलतम कथाकार विवेक मिश्र ने, जब मनीषा कुलश्रेष्ठ से उनके अब तक के साहित्यिक सफ़र पर बात करी, तो वो इंटरव्यू भी किसी कहानी से कम रोचक नहीं होना था . ये वाजिब भी है क्योंकि दोनो एक ही दौर के सफल युवा कथाकार भी हैं.
विवेक:-आपकी कहानियों को पढ़कर, आपसे मिलकर, बातचीत करके लगता है कि आपके जीवन में कला का बहुत महत्व है। आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में एक एस्थेटिक इन्क्लेनेशन है। क्या लेखन उसी रुझान की उपज है, या इसकी और कोई वजह है?
छोटे कस्बे से निकल कर फिर एयरफोर्स के माहौल में आए तो थोड़ा एस्थेटिक एक संक्रमण की तरह आ गया हो तो आ गया होमनीषा:-कला अपने शत प्रतिशत विशुद्ध रूप में तो मेरे जीवन में शुरु से नहीं थी. मैं लोक – कलाओं के ज़्यादा निकट रही. मेवाड़ के इलाके में मेरा बचपन बीता, जहाँ मीराँ के भजन लोक में अलग तरह से प्रचलित हैं. कई तरह के लोकनाट्य ‘गवरी’ और ‘वीर तेजाजी’ देखते हुए होश सँभाला है. अपने मन के भीतर उतरती हूँ तो मुझे मिलती है, एक कुतुहल प्रिय लड़की जो कठपुतलियों के खेल, बहुरूपिये, भवाई नृत्य आदि जैसी लोककलाओं के बीच बड़ी हो रही है, एक इतिहास के साए में पल रही है....किले, बावड़ियाँ जहाँ स्थापत्य और मूर्तिकला का उत्कृष्ट स्वरूप खेल – खेल में शामिल है. आईस – पाईस खेल रहे हैं हवेलियों में....बावड़ियों में उतर रहे हैं. मीराँ महोत्सव हो रहा है, देवीलाल सामर आ रहे हैं, कठपुतलियाँ बनाने का बाल शिविर लग रहा है लोककला मण्डल में, जहाँ न केवल हैण्ड पपेट बनानी है, अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है, प्रदर्शित भी करनी है.... उसके बाद कॉलेज में आकर कथक सीखा...किश्तों में, थोड़ा बहुत जयपुर घराना. लेकिन विधिवत 35 वर्ष की उम्र में कथक सीखा, जब बच्चे स्कूल जाने लगे. विशारद किया गुरु भगवान दास माणिक और मोहिनी जी की शिष्या होकर, कथक की रायगढ़ शैली में. नियमित मंच प्रदर्शन और नियमित रियाज़ जैसी स्थिति आ नहीं सकी क्योंकि ग्वालियर से तबाद्ला हो गया, मगर कथक से जुड़ाव हमेशा रहेगा.
एस्थेटिक ! मुझे तो अपना सब कुछ ‘गँवई’ और ‘प्राकृतिक’ लगता है. हो सकता है इस गँवई और प्राकृतिक का अपना सौन्दर्यबोध होता हो.
लेखन, मेरे लम्बे एकांत से उपजे कल्पना जगत का परिणाम है. जिला शिक्षा अधिकारी माँ और बी.डी.ओ. पिता हमेशा अपनी – अपनी जीपों में टूर पर रहते थे. मैं और मेरा भाई घर पर. किताबों के लिए पूरी लाईब्रेरी उपलब्ध थी, कोई सेंसर नहीं था, सो जो मिलता पढ़ डालते. आठवीं – नवीं में ही शंकर का ‘चौरंगी’ , बिमल मित्र का ‘साहिब बीवी और गुलाम’ , खाँडेकर का ‘ययाति’. हिन्द पॉकेट बुक से छपी अनूदित नॉबकॉव की ‘लॉलिटा’, स्वाइग की ‘एक अनाम औरत का ख़त’, हॉथार्न की ‘ द स्कारलेट लैटर’ पढ़ डाली थीं. और ऎसा नहीं था कि समझ नहीं आती थीं, खूब समझ आती थीं.
अब इस माहौल में तो कोई भी पलता, आखिरकार कुछ तो लिखता ही, और जो लिखता उसमें इसकी छवि होती न ! बाकि छोटे कस्बे से निकल कर फिर एयरफोर्स के माहौल में आए तो थोड़ा एस्थेटिक एक संक्रमण की तरह आ गया हो तो आ गया हो. बाकि हम लोग अपने भीतर कतई स्यूडो अंग्रेज़ीदाँ नहीं हो सकते. न मैं न मेरे पति अंशु. हम अब भी साधारण से जीव हैं.

विवेक मिश्र (बाएं) ललित शर्मा, अजय नावरिया, अंशु कुलश्रेष्ठ व मनीषा कुलश्रेष्ठ (दायें) के साथ
विवेक:-आप ठीक-ठीक अपने लेखन की शुरूआत कहाँ से मानती हैं और उस शुरुआत से लेकर आज तक इस सफ़र के महत्वपूर्ण पड़ाव कौन-कौन से हैं?
मेरे लेखन की शुरुआत ‘हंस’ के उस पत्र से हुई है, जिसे मैंने करगिल के बीच ही जुलाई 1999 में राजेन्द्र यादव को लिखा था
विवेक:-इस साहित्यिक सफ़र का चर्मोत्कर्ष कब आया?, या अभी लगता है कि उसे आना बाकी है?
शिगाफ़ लिखते हुए और अंत तक आते – आते मेरी धैर्यहीनता की वजह से मुझे कतई विश्वास नहीं था कि एक गैर कश्मीरी की तरफ से लिखे इस उपन्यास को ज़रा भी तवज्जोह मिलेगी.एक साल शांति रही, फिर यहाँ – वहाँ से आवजें उठीं...शिगाफ पढ़ा. शिगाफ पढ़ा? यार शिगाफ पढ़ा ! शिगाफ पढ़ना है! मुम्बई से कोई फिल्मकार फोन करके कहता ज्ञान रंजन जी ने कहा था इसे पढ़ने को, कोई कहता राजेन्द्र जी ने कहा ‘शिगाफ’ पढो, मगर सीधे मुझे किसी वरिष्ठ ने कुछ नहीं कहा, और मैं एकलव्य की तरह अपने एकांत में खुश होती रही. ( अपनी किताब पर फोन कैम्पेन चलाना, अपने वरिष्ठों पर मौखिक दबाव बनाने से ज़्यादा शर्मनाक मुझे कुछ नहीं लगता) मेरी किताबों की समीक्षाएँ आईं हैं, इसी ईमानदारी के साथ. पहला उपन्यास लिखकर मैं अपने पहले इम्तहान में पास थी बस ! इसलिए यह चरमोत्कर्ष कैसे हो सकता है, यह बस शुरुआत थी. हालांकि लोग डराते रहे, कि ‘शिगाफ’ से बेहतर लिखो तब ही लिखना, मगर मुझे यह बात नहीं जमी, मैं खराब भी लिखती रही तो भी लिखूँगी चाहे अपनी उँगलियों की खुशी के लिए ही सही. मैंने नॉवेला लिखा ‘शालभंजिका’ लोगों ने शिगाफ से तुलना की मगर उसे भी पसन्द किया उसके अपने फ्लेवर की वजह से. साहित्यिक सफर का चरमोत्कर्ष न ही आए तो अच्छा क्योंकि फिर ढलान शुरु होता है, हालांकि एक जीव विज्ञान से ग्रेजुएट होने के कारण जानती हूँ, मस्तिष्क में भी रचनात्मक न्यूरॉंस की एक उम्र होती है, फिर भी हम सब की नियति देवानन्द, मनोजकुमार की बाद की फिल्मों की सी हो जाती है......
मेरी नज़र चरम पर है नहीं है, मुझे लिखने में जब तक मज़ा आएगा लिखूँगी. नहीं तो हो सकता है, मैं फोटोग्राफी करने लग जाऊँ, कोरियोग्राफी करने लगूँ, वन्य जीवों पर काम करने लगूँ. हिन्दी में ही कहानी किस्से छोड़ विज्ञान – लेखन करने लगूँ.
विवेक:-अपनी रचनाओं में से यदि कहूँ किन को लिख कर कर आपको गहरी आत्म संतुष्टि हुई, या इससे उलट पूँछू कि अपनी ही किस रचना से आप संतुष्ट नहीं हैं और उसे समय आने पर दोबारा लिखना चाहेंगी?
मुझमें ‘मोहन राकेश’ जैसा धैर्य नहीं है कि अपनी किसी छपी – छपाई कृति को तीन बार लिखूँमनीषा:-ईमानदारी से कहूँ तो....अभी तक किसी रचना से गहरी आत्मसंतुष्टि नहीं हुई. सब को जब पढ़ती हूँ, तो लगता है, इसे यूँ लिखा जा सकता था. हाँ, ‘शिगाफ़’ में भी लगता है. ‘शालभंजिका’ मैं दुबारा लिखना चाहती हूँ, ख़ास तौर पर ‘पद्मा’ के चरित्र को गहरा करना चाहती हूँ. लेकिन मैं करूँगी नहीं, क्योंकि प्रेम के उस स्वरूप से मेरा बुरी तरह मोहभंग हो गया है. मैं जानती हूँ, मुझमें ‘मोहन राकेश’ जैसा धैर्य नहीं है कि अपनी किसी छपी – छपाई कृति को तीन बार लिखूँ...! मुझे तो लगा कि तीसरी बार लिख कर उन्होंने ‘लहरों के राजहंस’ को ओवरडन कर दिया था.
विवेक:-आपकी कहानियों के नारी चरित्र अन्य स्त्री लेखकों के नारी चरित्रों से अलग खड़े दिखाई देते हैं, सुख में-दुख में, शोषण में, बुरे से बुरे समय में भी वे कहीं न कहीं सुंदर हैं। वे अपनी नज़ाकत और नफ़ासत के साथ हैं, ऐसा क्यूँ?
विवेक:-आपकी रचनाओं में जीवन उदात्त रूप में उपस्थित है, पर समय और समाज की राजनैतिक स्थितियों और उसमें रचनाकार की अपनी विचारधारा बहुत स्पष्ट नहीं है, वह प्रछन्न है। कहीं-कहीं यथास्थितिवाद का समर्थन भी करती लगती है, आप इस पर क्या कहेंगी?
यह भीषण अविश्वास का दौर है....किस पर विश्वास प्रकट करूँ?मनीषा:-हाँ, जीवन ही सर्वोपरि है, बहुस्तरीयता में, अपने गुंजलों में. सवाल के दूसरे भाग से मेरी असहमति है. समय और समाज़ की राजनैतिक स्थितियाँ मेरी रचनाओं में समय से पूर्व एक पूर्वाभास की तरह आई हैं. जब खाप पंचायतों की तरफ से मीडिया सोया था, बल्कि मैं ‘खाप’ शब्द से अपरिचित थी, तब मैंने लोक पंचायत को लेकर ‘कठपुतलियाँ’ लिखी थी. अभी ‘मलाला’ पर हमला तो बहुत बाद में हुआ, हम लोगों को उसका नाम भी बाद में पता चला...मेरी कहानी ‘रक्स की घाटी -शबे फितना’ हंस के अगस्त अंक में आ गई थी. ‘शिगाफ’ तो है ही...रही बात मेरी राजनैतिक विचारधारा की ! कौनसी राजनैतिक विचारधारा ऎसी है जिसमें मैं अपना सम्पूर्ण विश्वास प्रकट कर सकूँ? यह भीषण अविश्वास का दौर है....किस पर विश्वास प्रकट करूँ?

समाधान की नीम हकीमाना पुड़िया मैं कभी नहीं बाँध सकतीवैसे तो किसी रचनाकार की राजनैतिक विचारधारा का चला कर, प्रकट तौर किसी कहानी या उपन्यास में आना लेखन में फूहडपन ही माना जाएगा. रही बात अपनी कथा के माध्यम से किसी सामाजिक राजनैतिक विषम स्थिति के प्रति अपना विरोध स्थूलता के साथ प्रकट करने की, या किसी कथानक के ज़रिए कोई नारा उछालने की मंशा तो मेरी आगे भी नहीं रहेगी, ऎसा करना होता तो अपने भीतर किसी प्रछन्न विचारधारा को आवेग में लाकर ‘शिगाफ’ में मैंने कश्मीर समस्या का कोई अव्यवहारिक हल पकड़ा दिया होता! वह सरल होता मेरे लिए, बहुत ही सरल, मेरा मन जानता न कि यह झूठ है, अव्यवहारिक है. फिर क्या वह पठनीय भी होता? और विश्वसनीय तो कतई नहीं होता. मेरे भीतर के कहानीकार का यह विश्वास मरते दम तक बना रहेगा कि मेरी कहानी ‘दिशा सूचक’ बोर्ड हो सकती है...कि ‘एक बेहतर, संभावित रास्ता इधर को ...’ मगर समाधान की नीम हकीमाना पुड़िया मैं कभी नहीं बाँध सकती. मेरे नारी पात्र अपनी शर्तों पर जीते हैं, अपनी तरह से विरोध दर्ज करवाते हैं, मगर उनके अपने मोह और कमज़ोरियाँ हैं...हाँ यह सच है कि उनमें से ज़्यादातर ‘घर’ नाम की पैरों के नीचे की ज़मीन को खोने से भय खाते हैं, मातृत्व के हाथों हारते हैं...... मुझे एक कहानीकार के तौर पर दबाव रहे हैं कि मैं अपना राजनैतिक रुझान स्पष्ट करूँ ! अब तो मैंने भी एक उम्र जी ली, संसार घूम लिया, मैं लेफ्ट, राईट, सेंटर सबकी आउटडेटेड, अव्यवहारिक, अवसरवादी नीतियों को देख चुकी, भारतीय राजनीति का बहुरंगा चेहरा किस से छिपा है? हमारे यहाँ भी लोग झण्डा वाम का, फण्डा सत्ता का, दिखावा सेकुलर होने का और कलाई पर कलावा बाँध घूमते हैं. क्या उनके राजनैतिक रुझान कनफ्यूज़िंग नहीं? क्योंकि मेरा ही नहीं इस अविश्वास के दौर में किस युवा का राजनैतिक रुझान क्या हो सकता है? ऎसे में अपॉलिटिकल होना ही सुझाता है, बिना झंडा उठाए या किसी झण्डे तले बैठे भी आप सही के साथ और गलत के विरोध में हो सकते हैं. हम किसी फ्रेम से बाहर, एक नए विचार की तलाश में निकले लोग हैं, जो विचार के नाम पर बँटना नहीं चाहते।
ऎसे में उदासीनता...डेलीबरेट नहीं विवशता है....फिर भी....अपॉलिटिकल न रहने देने का दबाव मुझ पर बना हुआ है. मैं जिस से जुड़ सकूँ ऎसी राजनैतिक विचारधारा को अब समय के हिसाब से अपडॆट होना होगा.
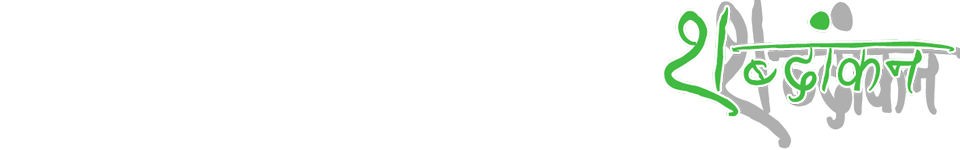




































2 comments:
Post a Comment